सूरदास की कविता की विशेषताऍं
[Surdas ki kavita ki visheshtaye] (हिंदी काव्य)
IGNOU MHD - 01 Free Solved Assignment
सूरदास की कविता की विशेषताऍं बताइए ।
उत्तर: सूरदास के काव्य की विशेषताऍं:
सूरदास भक्ति युग के प्रमुख कवि है। ये कृष्णभक्ति काव्य परंपरा के सिरमौर हैं। सूर ने भगवान कृष्ण के लोकरंजन स्वरूप को लेकर भक्ति, वात्सल्य तथा श्रृंगार का जैसा अनोखा वर्णन किया है वैसा अन्यन्न दुर्लभ है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का प्रमुख स्थान है। सूर्य की काव्यात्मक विशिष्टता और उत्कृष्टता का आधार है -
(क) संगीत का कलात्मक उपयोग।
(ख) ब्रजभूमि की लोकसंस्कृति का आत्मासातीकरण।
(ग) वात्सल्य चित्रण।
(घ) स्त्री-पुरुष संबंधों का स्वच्छंद चित्रण।
भक्तकवि सूरदास कृष्ण के उपासक हैं। कुछ लोग भक्ति को साधन एवं मोक्ष को साध्य मानते हैं, किंतु सूरदास की कृष्ण के प्रति भक्ति साध्य है, साधन नहीं । गोपियाँ मुक्ति का निरादर करती हैं, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, वे तो बस कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं । सूरदास जिस पुष्टिमार्गी भक्ति में दीक्षित थे, उसमें भी भक्ति को साधन न मानकर साध्य ही माना गया है । पुष्टिमार्गी होने के कारण सूर की भक्ति प्रेमाभक्ति थी।
सूर के काव्य में समर्पण को ही सब कुछ माना गया है। सूर ने अपने काव्य में उपास्य कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए उनके रूप व्यक्तित्व, परिवेश, क्रियाकलाप, लीला आदि का चित्रण सहज मानवीय रूप में किया है। सूरदास ने पुष्टिमार्गीय प्रेमाभक्ति को अपनाया है । कृष्ण प्रेममय है और प्रेम के वशीभूत होकर ही ब्रजभूमि में वे अवतरित हुए हैं । सूर की भक्ति स्वयं में साध्य है, कुछ और प्राप्त करने का साधन नहीं है ।
सूरदास ब्रजभाषा में कविता रचने वाले पहले प्रमुख कवि है। उन्होंने ब्रज प्रदेश को लोक संस्कृति और वाचिक परंपरा की उत्कृष्टता प्रदान की और उसे कलात्मक उत्कर्ष प्रदान किया। संगीतात्मकता उनके काव्य का अप्रतिम गुण हैं।
वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही सूरदास श्रीमद्भागवत में वर्णित कृष्ण कथा को गीत - संगीत में रूपांतरित करने लगे। श्रीमद्भागवत में कृष्ण के लोकमंगलकारी और लोकरक्षक व्यक्तित्व की भी कुछ छटाऍं और छवियाँ है। अतः सूरसागर में संकलित आपको सैकड़ों ऐसे पद हैं, जिनमें कृष्ण लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं।
सूरदास के काव्य में संगीत के नवोत्थान और मध्यकालीन भारत के लोकजागरण के बीच बड़ा गहरा संबंध है। सूरदास उस युग की नवोन्मेषकारी संस्कृतिक प्रक्रिया और नयी भावधारा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। सूरदास के काव्य में उनका मन रमता है राधाकृष्ण, गोप - गोपिका, नंद - यशोदा और ब्रज की हरी-भरी प्रकृति की जीवंत क्रियाओं और मनोरम रूपो के चित्रण में ।
सूर के चित्रण - शैली में ब्रज की लोक- संस्कृति लिपटी हुई चली आती है तथा सूर के स्वर संगीत में जनभाषा के रूप में ब्रजभाषा की मृदुता की और मधुरता की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। सूर के काव्य को नृत्य, रास, संगीत, गायकी और ब्रज लोकगीत के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में है। सूरदास ललित कलाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान और घनिष्ठ अंत क्रिया के साक्षी थे।
सूरदास की कविताओं में सूरदास उन जनभाषा में अपनी कविता रच रहे थे, जो साहित्यिक - संस्कृतिक दृष्टि से अपरिष्कृत और पिछड़ी हुई थी, यद्यपि अपनी प्रगीत परंपरा के लिहाज से ब्रजभाषा लोक कंठो में रची बसी हुई थी। और इसी वजह से सुमधुर हो गई थी। अगर भक्ति आंदोलन से सूरदास के काव्य को निकाल दिया जाए तो वह एकांगी और विकलांग प्रतीत होगा।
सूरदास समेत सभी कृष्णभक्त कवियों का एक ही लक्ष्य था - रस, आनंद और प्रेम की युगलमूर्ति राधाकृष्ण की लीला का गायन और इन कृष्णभक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण है । बड़े - बड़े भूपालों के बीच लोकव्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्रीकृष्ण नहीं है।
कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वह हास - विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र हैं।
(i) सूर के काव्य में सगुण - निर्गुण का द्वंद:
भक्त कवि सूरदास कृष्ण के लीलामय सगुण रूप के अनन्य भक्त हो गये, जबकि 'भ्रमरगीत' के उद्धव गोपी संवाद में ज्ञान बनाम भक्ति, सगुण बनाम निर्गुण की बहस अपने प्रखर रूप में व्यक्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि सूरदास नाथपंथियों, सिद्धों और संतों की दलिलों का खंडन कर रहे हैं। उद्धव - गोपी संवाद वस्तुतः निरगुनिया मत से सूर की मुठभेड़ का छाया - बिंब प्रतीत होता है। गोपियों की अश्रुपूरित, भावाकुल और करुण मनोदशा स्वयं में उद्धव को निरुत्तर करने, उन्हें चुप करने, खामोश करने की तार्किक क्षमता रखती है।
'भ्रमरगीत' को सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी अंश माना जाता है। ज्ञानयोग के प्रतिपक्ष में साकार उपास्य देव के लिए प्रेमभक्ति की भावना सूर के काव्य में निर्विवाद रूप से उपस्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर ने सगुण - निर्गुण के विवाद में ज्ञान या योगमार्ग को संकीर्ण, कठिन तथा नीरस बताया और भक्तिमार्ग को विशाल राजपथ जैसा सरल और सरस माना है।
सूर के काव्य में उनकी यही तर्क पद्धति है जो भोली-भाली गोपियों के संवाद के माध्यम से रसभरी भक्ति की रमणीयता से सराबोर है। सगुण - निर्गुण विवाद की यह द्वंदात्मकता ही भ्रमरगीत प्रसंग का प्राण है।
गोपियों की प्रेममग्न तन्मयता, विहलता और भावना में पगी तर्कशीलता के आगे अंततः उद्धव हार मान जाते हैं। उद्धव जब लौटकर मथुरा आते हैं और श्रीकृष्ण को अपनी यात्रा का वृतांत सुनाते हैं तो एक तरह से अपनी पराजय मान लेते हैं। सगुण - निर्गुण विवाद में उद्धव का यह चित्र प्रस्तुत कर सूरदास मानवीय संवेदना का एक भाव - विहल परिणाम दिखलाते हैं कि किस तरह गोपियों के आगे उद्धव हार कर लौटे हैं।
(ii) सूर के काव्य में प्रेमाभक्ति:
सूर के काव्य में प्रेमाभक्ति में पुष्टिमार्ग को श्रेष्ठ बताया था। पुष्टिमार्ग में भगवान के रूप में श्रीकृष्ण के परमानंद रूप की आराधना या उपासना की व्यवस्था की गई है। श्रीकृष्ण सौंदर्य, आनंद और रस के आगार हैं। सूरदास के उपास्य श्रीकृष्ण है, जिनके प्रति गहरा अनुराग और प्रेमपूर्ण भावावेग व्यक्त करने के लिए उनके रूप, व्यक्तित्व, परिवेश, क्रियाकलाप, लीलामय स्वरूप आदि का चित्रण सहज मानवीय संबंधों के गतिमान संदर्भो के बीच से किया गया हैं।
(iii) सूर की कविता में भाषा और रूप विधान:
ब्रजभाषा में काव्य - परंपरा का सूत्रपात सूरदास ने ही किया था। सूरदास के पहले ब्रजभाषा की साहित्यिक परंपरा का अस्तित्व था और सूरदास ने उस परंपरा से सीखकर अपनी भाषा और काव्य शैली का परिष्कार किया था। सूरदास का काव्य ब्रज प्रदेश की लोक - संस्कृति और उसकी वाचिक परंपरा से प्राण शक्ति खींचकर पला, बढ़ा और परिष्कृत हुआ था।
सूरदास के काव्य में बाल वर्णन हो या श्रृंगार वर्णन कृष्ण की मनोहर छवि चारों ओर विद्यमान है। श्रृंगार वर्णन में जो स्वंच्छदता और उन्मुक्तता सूर के काव्य में मिलती है, वह न पहले मौजूद थी और न ही बाद में यह परंपरा सुरक्षित रह सकी। सूर के कृष्ण और गोपियाँ स्वच्छंद है, लोकबंधन में जकड़े हुए नहीं है। सूरदास ने अपने पदों में वात्सल्य और श्रृंगार रस की अजस धारा बहा दी हैं ।
(iv) सूर का वात्सल्य वर्णन:
सूर के काव्य में जिस बाल मनोदशाओ और बालक्रीड़ाओं का वर्णन है, वह अन्यत्र दुर्लभ ही है। 'सूरदास' में कृष्ण जन्म की आनंद बधाई के दृश्यचित्रण में बाललीला का अंकन शुरू हो जाता है। बालकृष्ण का एक रूप है - पलक हरि मूँदि लेते हैं, कबहुँ अधर फरका लेते है। दूसरा रूप है - "उभय पलक पर' स्वपन जागरण। तीसरा रूप है - हाथ और पाँव का अंगूठा मुँह में लेना।
पालना झूलने, यशोदा की गोद में खेलने, स्तनपान करने, घुटनों के बल चलने, डगमगा कर गिर पड़ने, मथानी की आवाज के साथ नाचने का प्रयत्न करने, दूध न पीने का हठ करने, चोटी बढ़ने के प्रलोभन पर दूध पीने, माँ द्वारा चंद्रमा दिखाये जाने पर चंद्रमा माँगने का हठ करने, माखन चोरी के लिए तरह-तरह की बालोचित युक्तियाँ निकालने - इस प्रकार की सैकड़ों बालोंचित क्रीड़ाओ के चित्र सूरसागर में भरे पड़े हैं। सूक्ष्म निरीक्षणों से भरापूरा सूर का बालवर्णन मनोविज्ञान की अनेक प्रक्रियाओं को दर्शाता है। सूरदास कविता में ब्रज की लोक संस्कृति बोलती प्रतीत होती है। कृष्ण की बाललीला का चित्रण हो या रासलीला का सर्वत्र प्रेम का ही साम्राज्य है।
(v) सूरदास की विशेषता:
सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मौलिकता। उन्होंने ब्रजभाषा को सुघड़ रूप दे दिया। सूरदास की दूसरी विशेषता उनकी स्वच्छंदता। वे अपने आराध्य कृष्ण और गोपियों की भांति सर्वथा स्वच्छंद ही विचरे। उनका हृदय सीमित है, पर अनुभूतियाँ असीम है । वे अपनी बंद ऑंखों से भी मानव हृदय का कोना - कोना झाँक आए हैं।
***

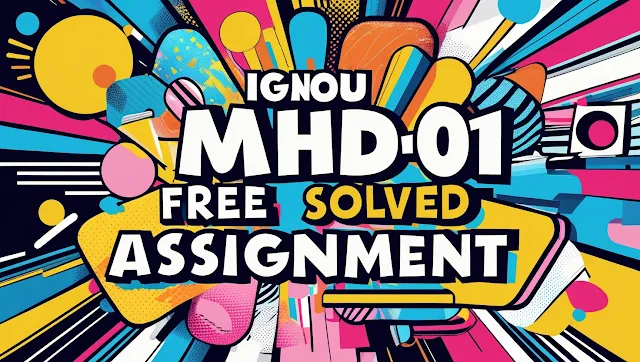
Post a Comment
Kindly give your valuable feedback to improve this website.